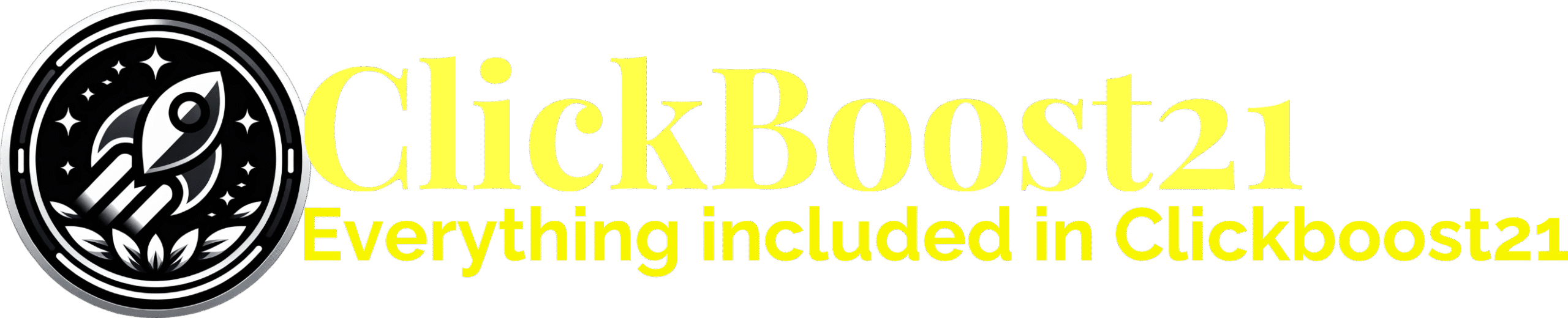भारत के तटों के पार, सुंदरबन डेल्टा के सुस्त चैनलों से लेकर मुंबई के स्टिफ़ल्ड क्रीक्स तक, मैंग्रोव एक बाधा बनाते हैं भूमि और समुद्र के बीच। ये तटीय जंगल भारत के जलवायु लचीलापन, जैव विविधता संरक्षण और तटीय समुदायों के सशक्तिकरण की खोज में महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि, शहरी विस्तार, जलवायु परिवर्तन और विकास के सामने, भारत के मैंग्रोव कैसे जीवित हैं – और उनकी रक्षा कौन कर रहा है?
मैंग्रोव्स मैटर
मैंग्रोव दलदल जंगल वाले आर्द्रभूमि होते हैं जिनकी विशेषता पेड़ों की विशेषता होती है जो खारा पानी को सहन कर सकते हैं। वे प्राकृतिक बाधाओं के रूप में काम करते हैं, तटीय समुदायों को चक्रवातों, ज्वारीय वृद्धि और कटाव से बचाते हैं। 2004 के हिंद महासागर सुनामी और बंगाल की खाड़ी में आवर्ती चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, मैंग्रोव को तटीय बुनियादी ढांचे और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है और हजारों लोगों की जान बचाई है।
जैव विविधता संरक्षण में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव मछली, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रजनन और नर्सरी के मैदान प्रदान करते हैं। ये नमक-सहिष्णु जंगल भी महत्वपूर्ण मात्रा में नीले कार्बन (समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन) को संग्रहीत करते हैं, जिससे उनकी जड़ों और मिट्टी में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाकर जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।
भारत के मैंग्रोव 4,900 वर्ग किलोमीटर से अधिक को कवर करते हैं, जिसमें अन्य राज्यों में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, और कर्नाटक के तटों के साथ एस्टुरीज, डेल्टास, और अन्य राज्यों में शामिल हैं। तटीय समुदायों के लिए, विशेष रूप से पारंपरिक मछुआरों और शहद इकट्ठा करने वाले, मैंग्रोव आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़े हुए हैं।
फिर भी वे शहरी विस्तार, एक्वाकल्चर, प्रदूषण और बदलते जलवायु पैटर्न से तेजी से धमकी दे रहे हैं। यह अकेले भारत में ऐसा नहीं है: दुनिया भर में, सभी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से आधे से अधिक 2050 तक गिरने का खतरा है, ए के अनुसार हाल की रिपोर्ट प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ से (IUCN)।
इन बढ़ते खतरों के बावजूद, हालांकि, भारत भी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरणादायक प्रयासों की बढ़ती संख्या का उपरिकेंद्र है। स्टूवर्डशिप, वैज्ञानिक समर्थन और नीति का ध्यान देने के सही मिश्रण के साथ, वे दिखा रहे हैं कि मैंग्रोव केवल जीवित नहीं रह सकते हैं: वे पनप सकते हैं।
तमिलनाडु में मैंग्रोव
हाल के वर्षों में, तमिलनाडु में मैंग्रोव को बहाल करने के प्रयासों ने उल्लेखनीय प्रगति देखी है, जो सरकारी पहल, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक योजना के संयोजन से प्रेरित है। एक बार झींगा की खेती, औद्योगिक प्रदूषण और परिवर्तित जल विज्ञान द्वारा गंभीर रूप से अपमानित होने के बाद, राज्य के स्थलों और तटों को आज एक धीमी लेकिन स्थिर वापसी देखी जा रही है।
ग्रीन तमिलनाडु मिशन और अन्य तटीय बहाली कार्यक्रमों के तहत, अन्य लोगों के बीच तंजावुर, तिरुवरुर और कुडलोर के जिलों ने मैंग्रोव कवर का काफी विस्तार किया है। नतीजतन, तमिलनाडु ने अपनी मैंग्रोव सीमा को लगभग दोगुना कर दिया – 2021 और 2024 के बीच 4,500 हेक्टेयर से 9,000 हेक्टेयर से अधिक तक – और भारत में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की वसूली का नेतृत्व कर रहा है।

2017 की शुरुआत में, स्थानीय ग्राम समितियों और तमिलनाडु वन विभाग के सहयोग से चेन्नई में सुश्री स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने मुथुपेटाई के पट्टुवनाची मुहाना में 115 हेक्टेयर अपमानित मैंग्रोव को बहाल करने के लिए एक परियोजना शुरू की। पूरी तरह से साइट आकलन और सामुदायिक जुड़ाव के बाद, टीम ने ज्वारीय प्रवाह को बहाल करने के लिए 19 प्रमुख नहरों को खोदा। फिर टीम के सदस्यों ने 4.3 लाख से अधिक लगाया एविसेनिया मुथुपेटाई से बीज और 6,000 राइजोफोरा Pichavaram से प्रचारक, एक बार-स्थिर परिदृश्य को एक संपन्न मैंग्रोव जंगल में सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करते हैं।
फिर भी तमिलनाडु की एक और सफलता की कहानी है एक हरे रंग की बेल्ट की बहाली चेन्नई में कज़िपहटुर में बकिंघम नहर के पास मैंग्रोव। ग्रीन तमिलनाडु मिशन के तहत, वन विभाग ने वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद से 2024 में पांच प्रजातियों से 12,500 मैंग्रोव रोपाई लगाए। बहाली में इनवेसिव को हटाना शामिल था प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा चक्रवातों और तूफान की वृद्धि के खिलाफ चेन्नई की प्राकृतिक ढाल को बहाल करने के लक्ष्य के साथ, मैंग्रोव रोपण से पहले खरपतवार।
मुंबई में संरक्षण
2025 की शुरुआत में, अमेज़ॅन के राइट नाउ क्लाइमेट फंड ने जल्दबाजी पुनर्जनन और बृहानमंबई नगर निगम के साथ भागीदारी की, जो मुंबई में थान क्रीक के साथ $ 1.2 मिलियन (24 जुलाई, 2025 को रुपये 10.3 करोड़ रुपये) लॉन्च करने के लिए, जो कि 180 के लिए आवश्यक मैनग्रोव जंगलों और मडफ्लैट्स को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से था।
इस परियोजना ने शहरी सफाई के साथ पारिस्थितिक बहाली को संयुक्त किया: कचरा बूम नामक बायोडिग्रेडेबल बाधाओं को प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें तीन वर्षों में कम से कम 150 टन प्लास्टिक के संग्रह को लक्षित किया गया था। इसके साथ ही, इस पहल ने लगभग 3.75 लाख मैंग्रोव पौधे लगाने की योजना बनाई है, फ्लेमिंगोस के लिए नया निवास स्थान बना रहा है और स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना, विशेष रूप से महिलाओं को रोपण और रखरखाव गतिविधियों में भुगतान किए गए रोजगार प्रदान करके।
पारिस्थितिक वसूली और सामाजिक-आर्थिक लचीलापन दोनों पर ध्यान केंद्रित करके, यह परियोजना यह उदाहरण देती है कि कॉर्पोरेट-समर्थित, प्रकृति-आधारित समाधान भारत के तेजी से शहरी तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
गुजरात की सफलता
गुजरात राज्य तटरेखा आवास और मूर्त आय योजना के लिए भारत सरकार की मैंग्रोव पहल के तहत मैंग्रोव बहाली में एक राष्ट्रीय नेता बन गया है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत, गुजरात ने दो साल में 19,000 हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव लगाए हैं, जो केंद्र सरकार के 54,000 हेक्टेयर के पांच साल के लक्ष्य को पार कर गया है।

इस प्रयास का लक्ष्य कच्छ और तटीय सौराष्ट्र क्षेत्रों में तटीय लचीलापन का पुनर्निर्माण करना है, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका को समान रूप से समर्थन देना, इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना, और देश के नीले कार्बन लक्ष्यों में योगदान देना।
गुजरात पहले से ही भारत के मैंग्रोव कवर के 23.6% का घर है और वर्तमान में इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे मजबूत योजना और रणनीतिक तटीय मानचित्रण जल्दी से बहाली के प्रयासों में मदद कर सकते हैं।
भारत के तटीय समुदायों की ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि मैंग्रोव संरक्षण न केवल संभव है, बल्कि वास्तव में अच्छी तरह से चल रहा है। आशा की ऐसी कहानियां आदर्श बननी चाहिए, अपवाद नहीं।
चूंकि जलवायु परिवर्तन और बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियाँ हमारे तटों को तबाह करती रहती हैं, जो कि अवशेषों की रक्षा करने और जो खो गया है उसे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता कभी भी अधिक जरूरी नहीं रही है। मैंग्रोव तूफानों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है, और वे मत्स्य पालन को भी आश्रय देते हैं और कार्बन को स्टोर करते हैं।
प्रिया रंगनाथन एक डॉक्टरेट छात्र और शोधकर्ता हैं जो अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (एटीआरईई), बेंगलुरु में हैं।